सीबीएसई की नई परीक्षा: शहरी उन्नति, ग्रामीण चुनौतियाँ
CAREER COUNSELING WITH CHAIFRY
Chaifry
6/26/20251 min read
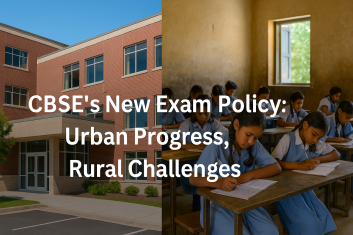
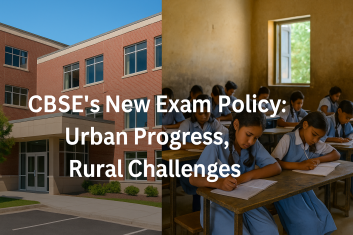
26 जून, 2025 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 2026 से कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं को साल में दो बार आयोजित करने की एक परिवर्तनकारी नीति की घोषणा की है । यह सुधार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना है, लचीलापन, कौशल विकास और परीक्षा के तनाव को कम करना। नई प्रणाली के तहत, छात्र फरवरी और मई में परीक्षाओं का सामना करेंगे, जिसमें अपने सर्वश्रेष्ठ अंकों को बनाए रखने का विकल्प होगा। मूल्यांकन संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जिसमें 50% प्रश्न दक्षता-आधारित होंगे—जैसे बहुविकल्पी और अनुप्रयोग-उन्मुख कार्य—और 20-30% आंतरिक मूल्यांकन जैसे प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल शामिल होंगे।
यह एनईपी 2020 के दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो रटने की शिक्षा से दूर होकर अधिक समग्र, छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है। इसका प्रभाव समझने के लिए, हमें यह देखना होगा कि यह नीति शहरी और ग्रामीण स्कूलों पर अलग-अलग कैसे प्रभाव डालती है, इसका अंतर्निहित उद्देश्य क्या है, और यह भारत के शैक्षिक भविष्य को आकार देने की क्षमता रखती है या नहीं।
शहरी भारतीय स्कूलों पर प्रभाव
शहरी स्कूल, विशेष रूप से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में, इस नीति को प्रभावी ढंग से अपनाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। उन्नत बुनियादी ढांचे—स्मार्ट कक्षाएं, डिजिटल उपकरण और प्रशिक्षित संकाय—के साथ, ये संस्थान दक्षता-आधारित शिक्षा को सहजता से एकीकृत कर सकते हैं। व्यावहारिक कौशल और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करना उनकी मौजूदा जोर को प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे जेईई और नीट के लिए छात्रों को तैयार करने के साथ पूरक करता है। उदाहरण के लिए, चेन्नई के एक निजी स्कूल ने पहले ही प्रोजेक्ट-आधारित मूल्यांकन का पायलट चलाया है, जिसमें छात्र सतत शहरी मॉडल डिजाइन करते हैं, एक दृष्टिकोण जो अब द्विवार्षिक प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से अपनाया गया है। "दो में से सर्वश्रेष्ठ" स्कोरिंग विकल्प शहरी छात्रों को और सशक्त बनाता है, जो बीमारी जैसे अप्रत्याशित झटकों के खिलाफ एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है। फरवरी में खराब प्रदर्शन करने वाला छात्र मई की परीक्षा का उपयोग करके सुधार कर सकता है, ऑनलाइन ट्यूशन जैसे संसाधनों का लाभ उठाते हुए, जो शहरों में व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। गुड़गांव के एक स्कूल का 2024 का केस स्टडी इस लाभ को रेखांकित करता है: एक दोहरे-मूल्यांकन मॉडल को अपनाने के बाद, इसने 90% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले छात्रों में 12% की वृद्धि दर्ज की, यह दर्शाता है कि शहरी स्कूल इस नीति के लाभों को अधिकतम कैसे कर सकते हैं।
यह लचीलापन शहरी स्कूलों की वैश्विक आकांक्षाओं के साथ भी मेल खाता है। विदेशों में सीबीएसई स्कूलों के लिए एक वैश्विक पाठ्यक्रम की शुरुआत—जिसमें एआई, वित्तीय साक्षरता और पर्यावरण अध्ययन जैसे विषय शामिल हैं—छात्रों को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए तैयार करता है। बेंगलुरु के एक स्कूल ने हाल ही में एक एआई मॉड्यूल लॉन्च किया, जिसमें छात्रों ने सरल चैटबॉट बनाए, एक कौशल जो दुनिया भर के विश्वविद्यालयों द्वारा मूल्यवान है। इस तरह के नवाचार एक मिसाल कायम कर सकते हैं, अन्य शहरी स्कूलों को भविष्योन्मुखी पाठ्यक्रम अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। हालांकि, एक दूसरा पहलू भी है। दोहरी परीक्षा प्रणाली शहरी छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को तीव्र कर सकती है, क्योंकि दोनों प्रयासों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए दबाव बढ़ सकता है। माता-पिता ने चिंता जताई कि उच्च औसत अंकों के कारण कॉलेज प्रवेश कटऑफ बढ़ सकता है, जिससे नए दबाव पैदा हो सकते हैं। निजी शहरी स्कूल खुद को "परीक्षा-अनुकूल" के रूप में विपणन कर सकते हैं, जिससे शहरों के भीतर कम संसाधन वाले सरकारी स्कूलों के साथ अंतर और बढ़ सकता है।
The new CBSE Class 10 board exam policy, effective from the 2026 academic session, introduces a biannual exam system with the following key points:
1. Two Exam Phases:
- Phase 1 (February-March): Mandatory for all Class 10 students.
- Phase 2 (May): Optional, for students seeking to improve their scores or for supplementary exams (e.g., for those who fail in up to two subjects). The best score from the two phases is retained.
2. Assessment Structure:
- Exams cover the full syllabus with no changes to textbooks.
- Question papers emphasize competency-based learning: 50% competency-based questions or MCQs, 30% descriptive questions, and 20-30% internal assessments (including practicals, projects, or portfolios).
- A 9-point grading system is used for evaluation.
ग्रामीण भारतीय स्कूलों पर प्रभाव
इसके विपरीत, ग्रामीण स्कूलों को भयावह चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो नीति की सफलता में बाधा डाल सकती हैं। भारत की 65% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में, शिक्षा प्रणाली पुरानी कमी और तार्किक बाधाओं से जूझ रही है। कई स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली नहीं हैं, इंटरनेट एक्सेस की तो बात ही छोड़िए, जो दक्षता-आधारित मूल्यांकन और ऑनलाइन रिकॉर्ड-कीपिंग के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण हैं। नीति का निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर निर्भरता—सेल्फ-सेंटर्स पर प्रतिबंध—का मतलब है कि ग्रामीण छात्रों को स्थानों तक पहुंचने के लिए घंटों की यात्रा करनी पड़ सकती है। ओडिशा के एक ग्रामीण छात्र के लिए, यह एक दिन की यात्रा हो सकती है, जो वैकल्पिक मई परीक्षा में भागीदारी को हतोत्साहित करती है। शिक्षकों की कमी इस मुद्दे को और जटिल बनाती है। 2024 की शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बिहार जैसे राज्यों में ग्रामीण स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात 50:1 से अधिक है, जबकि राष्ट्रीय औसत 24:1 है। अधिक विस्तारित शिक्षकों, जो पारंपरिक तरीकों के आदी हैं, को प्रशिक्षण के बिना नई मूल्यांकन तकनीकों को अपनाने में कठिनाई हो सकती है।
वित्तीय और सांस्कृतिक बाधाएं और जटिलता जोड़ती हैं। सीबीएसई की दोनों परीक्षाओं के लिए अग्रिम शुल्क संग्रहण ग्रामीण परिवारों पर दबाव डाल सकता है, जिनमें से कई गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। हालांकि सटीक लागतें अस्पष्ट हैं, हितधारक वृद्धि की आशा करते हैं, संभवतः कम आय वाले छात्रों को दूसरा प्रयास करने से बाहर कर सकते हैं, जब तक कि सब्सिडी प्रदान नहीं की जाती। सांस्कृतिक रूप से, रटने की शिक्षा में डूबे ग्रामीण छात्रों को दक्षता-आधारित प्रश्नों को अलगावित करने वाला लग सकता है। शहरी-शैली के संसाधनों जैसे कोचिंग तक पहुंच के बिना, वे पीछे रहने का जोखिम उठाते हैं। 2023 के वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट के आंकड़े दिखाते हैं कि ग्रामीण छात्र पहले से ही महत्वपूर्ण कौशल में पिछड़ रहे हैं, एक अंतर जो यह नीति ओर बढ़ा सकती है यदि इसे संबोधित नहीं किया गया। मोबाइल परीक्षा केंद्रों या एनजीओ के साथ शिक्षक प्रशिक्षण साझेदारी जैसे समाधान इन मुद्दों को कम कर सकते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में शहरी छात्रों को अनुपातहीन रूप से लाभ हो सकता है।
छात्र-केंद्रित या परिणाम-उन्मुख?
यह असमानता एक गहरे सवाल को जन्म देती है: क्या यह नीति वास्तव में छात्रों के लिए है, या यह सीबीएसई द्वारा परिणाम-उन्मुख कदम है? इसका एनईपी 2020 के समग्र लक्ष्यों के साथ संरेखण एक छात्र-केंद्रित फोकस का सुझाव देता है। मूल्यांकन को विविधता प्रदान करके और एकल-परीक्षा दबाव को कम करके, इसका उद्देश्य लचीलापन और सीखने को बढ़ावा देना है। सीबीएसई के ऐतिहासिक पास दर, लगातार 90% से ऊपर, यह दर्शाते हैं कि यह केवल उच्च आंकड़ों का पीछा नहीं कर रहा है। छात्रों को दो मौके विकास को प्रोत्साहित करते हैं, न कि केवल ग्रेड को। संशयवादी तर्क देते हैं कि "दो में से सर्वश्रेष्ठ" प्रणाली ग्रेड मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती है, सीबीएसई की प्रतिष्ठा को बढ़ा सकती है बिना सीखने में सुधार के भी। शिक्षक कार्यभार और छात्र थकान में वृद्धि की आशंका जताते हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो नए प्रारूप के लिए तैयार नहीं हैं। यदि शहरी छात्र लाभों पर हावी होते हैं, तो नीति समानता पर प्रकाशिकी को प्राथमिकता दे सकती है। फिर भी, इसका इरादा सुधार में निहित लगता है, जिसमें समान कार्यान्वयन मुख्य चुनौती है।
दीर्घकालिक प्रभाव
यह नीति भारतीय शिक्षा को गहराई से नया आकार दे सकती है। कौशल पर जोर देकर, यह छात्रों को एक गतिशील नौकरी बाजार और उच्च शिक्षा के लिए तैयार करेगी, जहां अनुकूलनशीलता की सराहना की जा रही है। विश्वविद्यालय प्रवेश मानदंडों को समायोजित कर सकते हैं, और नियोक्ता व्यावहारिक अनुभव वाले स्नातकों को पसंद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वित्तीय साक्षरता मूल्यांकन में उत्कृष्टता प्राप्त करने वाला छात्र बैंकिंग भर्तीकर्ताओं को आकर्षित कर सकता है। यह नीति सीबीएसई से परे लहर पैदा कर सकती है, राज्य बोर्डों को समान मॉडल अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिससे लचीली शिक्षा की ओर राष्ट्रीय बदलाव हो सकता है। वैश्विक स्तर पर, यह ब्राजील जैसे देशों को, जिनमें शहरी-ग्रामीण विभाजन हैं, मूल्यांकन पर पुनर्विचार करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। हालांकि, इसकी सफलता असमानताओं को पाटने पर निर्भर करती है। यदि ग्रामीण स्कूल पिछड़ते हैं, तो सामाजिक-आर्थिक अंतर बढ़ सकता है, जिससे लाखों युवाओं के अवसर सीमित हो सकते हैं। बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण में निवेश के साथ, यह राष्ट्रीय मानकों को ऊंचा कर सकता है, भारत को एक शैक्षिक नवप्रवर्तक के रूप में स्थापित कर सकता है।
