लिखने की कला: मिट्टी, संस्कृति और ज़िंदगी का जादू
CHAIFRY POT
लिखने की कला: भाग -1
6/26/20251 min read
लिखना कोई साधारण काम नहीं है। यह वह जादू है, जो शब्दों को दिल से दिल तक पहुँचाता है। चाहे हिंदी हो, पंजाबी हो, तमिल हो, या कोई और भाषा, लेखन अपनी मिट्टी की सोंधी खुशबू, संस्कृति की गहराई, और लोगों की ज़िंदगी की सच्चाई को साथ लाता है। यह एक ऐसी कला है, जो हमें दुनिया को सिर्फ़ देखने नहीं, बल्कि महसूस करने की ताकत देती है। यह लेख उस जादू की बात करता है—कैसे शब्द हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं, हमारी कमियों और अच्छाइयों को उजागर करते हैं, और प्रकृति व संस्कृति को जीवंत बनाते हैं। लिखना ऐसा है जैसे किसी नदी के किनारे बैठकर उसका बहना देखना। हर शब्द एक बूँद है, जो अपने साथ कोई कहानी, कोई एहसास लिए चलता है। लेखक जब कलम उठाता है, तो वह सिर्फ़ कागज़ पर अक्षर नहीं उकेरता; वह अपने गाँव की गलियों, शहर की चहल-पहल, और मिट्टी की महक को शब्दों में ढालता है।
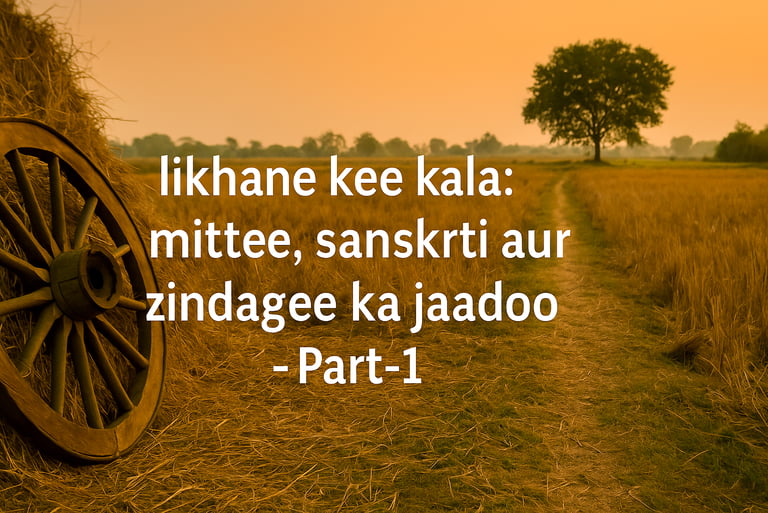
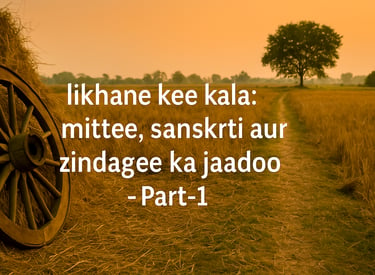
चाहे वह कविता हो, कहानी हो, निबंध हो, या डायरी का एक पन्ना, हर शब्द उस जगह, उस पल, और उस इंसान की ज़िंदगी का टुकड़ा होता है। हिंदी में लिखना तो जैसे घर की चौखट पर बैठकर माँ के हाथ की रोटी खाने जैसा है—सादा, अपनापन भरा। खड़ीबोली, जो हमारी रोज़मर्रा की हिंदी है, गाँव की पगडंडियों से लेकर शहर की चमकती सड़कों तक हर जगह बसती है। इसमें दादी की कहानियों का ठाठ है, तो मेट्रो में बैठे नौजवान की बातें भी। इसकी सहजता हर दिल को छू लेती है।
क्या आपने कभी बारिश की पहली बूँद से उठने वाली मिट्टी की खुशबू को सूँघा है? वह महक जैसे बचपन की यादों को जगा देती है। लेखन में भी वही सोंधी खुशबू होती है। जब लेखक अपनी धरती की बात करता है, तो वह सिर्फ़ जगह का नाम नहीं लेता, वह उसकी आत्मा को शब्दों में पिरोता है। प्रेमचंद की कहानियाँ इसका जीता-जागता सबूत हैं। उनकी ‘ईदगाह’ में हामिद की मासूमियत और दादी के लिए उसका चिमटा खरीदने का त्याग आपको गाँव की चौपाल तक ले जाता है। आप उस मिट्टी को छू सकते हैं, उसकी सादगी को जी सकते हैं। यशपाल की ‘दुख का अधिकार’ भी कुछ ऐसा ही जादू करती है। उनकी कहानियाँ गाँव की ज़िंदगी, सामाजिक असमानता, और छोटी-छोटी खुशियों को इतनी सच्चाई से बयान करती हैं कि आप उनके किरदारों के साथ हँmees.
पंजाबी साहित्य में भी यह मिट्टी की खुशबू खूब झलकती है। पंजाब के खेतों की हरियाली, लहलहाती फसलों का उल्लास, और गाँव की सादगी को लेखकों ने अपनी रचनाओं में बखूबी उतारा है। अमृता प्रीतम की ‘पिंजर’ में पंजाब के गाँवों की ज़िंदगी और औरतों की पीड़ा को इतनी गहराई से दर्शाया गया है कि आप उस माहौल में डूब जाते हैं। उनकी कविता ‘अज्ज आखां वारिस शाह नूं’ बँटवारे की त्रासदी के बीच भी पंजाब की धरती और उसकी हरियाली की पुकार है। शिव कुमार बटालवी की कविताएँ, जैसे ‘माये नि माये’, पंजाब के खेतों और नदियों को गीतों की तरह पेश करती हैं, जहाँ आप लहलहाते खेतों की ताज़गी महसूस करते हैं। नानक सिंह की ‘चित्रलेखा’ में पंजाब के गाँवों की मेहनत, सुख-दुख, और हरियाली इतनी खूबसूरती से उभरती है कि आप उन गलियों में चल पड़ते हैं।
हर भाषा की अपनी खुशबू है, मगर एहसास एक-सा है। तमिल कविता में समंदर की लहरें और मंदिर की घंटियाँ गूँजती हैं। अंग्रेज़ी में लिखने वाला अपनी गलियों की चमक या उदासी को उकेरता है। बंगाली में रवींद्रनाथ टैगोर की कविताएँ बंगाल की नदियों और खेतों को जीवंत करती हैं। यही लेखन का कमाल है—यह अपनी ज़मीन से जुड़ा रहता है, फिर भी इसका जादू हर दिल तक जाता है।
लिखना सिर्फ़ शब्दों का खेल नहीं, यह संस्कृति को सहेजने का ज़रिया है। हमारे त्योहार, रस्में, गीत, और कहानियाँ—यह सब लेखन में समा जाता है। हिंदी साहित्य में सूरदास की भक्ति कविताएँ कृष्ण की लीलाओं और भक्ति के रस से भरी हैं। कबीर के दोहे, जैसे “ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय”, सादगी और प्रेम की याद दिलाते हैं।
पंजाबी साहित्य में गुरु नानक देव जी की वाणी, जो गुरु ग्रंथ साहिब में है, पंजाब की आध्यात्मिकता और सादगी को दर्शाती है। उनकी शिक्षाएँ—“नाम जपो, किरत करो, वंड छको”(ईश्वर का नाम जपें, मेहनत करके जीविका कमाएं और अपनी कमाई को दूसरों के साथ मिल-बांटकर खाएं")—पंजाब के गाँवों की आत्मा हैं। अमृता प्रीतम की कविताएँ लोहड़ी के जश्न और लोकगीतों की खुशी को उजागर करती हैं। शिव कुमार बटालवी प्रेम और विरह को पंजाब की प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। नानक सिंह की कहानियाँ गाँवों की सामाजिक ज़िंदगी को सामने लाती हैं।
आधुनिक लेखक भी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। हरिवंश राय बच्चन की ‘मधुशाला’ में जीवन का फलसफा और संस्कृति का रंग है। उनकी पंक्तियाँ, “मधुशाला की मधुर माया”, हमें एकता का एहसास देती हैं। मैथिलीशरण गुप्त की ‘भारत-भारती’ देशप्रेम और संस्कृति की गहराई को उजागर करती है। आज की पीढ़ी ब्लॉग और सोशल मीडिया पर दिल्ली की चाट, होली के रंग, या दादी की कहानियों को लिखकर संस्कृति को ज़िंदा रखती है।
प्रकृति लेखन का अभिन्न हिस्सा है। सुमित्रानंदन पंत की कविताएँ हिमालय की खूबसूरती को जीवंत करती हैं। जयशंकर प्रसाद की ‘कामायनी’ में प्रकृति और मानव का गहरा रिश्ता दिखता है। महादेवी वर्मा की “मैं नीर भरी दुख की बदली” में बादल और बारिश मानव भावनाओं के प्रतीक बनते हैं। पंजाबी साहित्य में शिव कुमार बटालवी की ‘लूणा’ पंजाब के खेतों में ले जाती है। अमृता प्रीतम और नानक सिंह की रचनाएँ पंजाब की हरियाली और किसानों की मेहनत को उजागर करती हैं। लेखक जब प्रकृति की बात करते हैं, तो वह सिर्फ़ पेड़-पौधों का ज़िक्र नहीं करते, वह उस एहसास को बयान करते हैं, जो प्रकृति देती है—चाहे बारिश की बूँदें हों, सूखे खेत हों, या पहाड़ों की चुप्पी।
लेखन का सबसे बड़ा हिस्सा है लोगों की ज़िंदगी। सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ की ‘राम की शक्ति पूजा’ में मानव की आंतरिक ताकत झलकती है। फणीश्वरनाथ रेणु की ‘मारे गए गुलफाम’ में गाँव की मासूमियत और कमियाँ इतनी खूबसूरती से उकेरी गई हैं कि आप उस गाँव का हिस्सा बन जाते हैं। भैरव प्रसाद गुप्त की ‘सतह से उठता हुआ आदमी’ मेहनतकशों की उम्मीद दिखाती है। अमृतलाल नागर की ‘बूँद और समुद्र’ आम ज़िंदगी की छोटी-छोटी बातों को जीवंत करती है। पंजाबी में नानक सिंह की ‘पवित्र पापी’ गाँव की ज़िंदगी को सादगी से दर्शाती है। अमृता प्रीतम की ‘पिंजर’ औरतों की ताकत और पीड़ा को बयान करती है। शिव कुमार बटालवी की कविताएँ पंजाब के गाँवों को प्रेम और विरह के रंग में रंगती हैं। लेखक गरीब की हिम्मत, अमीर की खालीपन, हर ज़िंदगी को शब्दों में पिरोता है।
हिंदी की खड़ीबोली में लिखना दोस्त से दिल की बात करने जैसा है। यह भाषा गाँव की चौपाल से लेकर शहर की कॉफी शॉप तक बोली जाती है। इसमें वह गर्माहट है, जो हर दिल को जोड़ती है। धर्मवीर भारती की ‘गुनाहों का देवता’ प्रेम और उलझनों को इतनी सादगी से बयान करती है कि पाठक खो जाता है। पंजाबी में भी अमृता प्रीतम, शिव कुमार बटालवी, और नानक सिंह की रचनाएँ गाँव की ज़िंदगी को दिल तक पहुँचाती हैं।
आज का दौर डिजिटल है। लोग ब्लॉग, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लिखते हैं। कोई 280 शब्दों में कहानी कहता है, तो कोई कविता। गुलज़ार जैसे लेखक अपनी कविताओं, जैसे “दिल ढूँढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन”, में आधुनिकता और परंपरा का मेल लाते हैं। उनकी ‘रात पश्मीने की’ में पंजाब की ठंड और सादगी का अहसास है।
लेखन का भविष्य सुनहरा है। जब तक इंसान हैं, कहानियाँ होंगी। यह कला हमें जड़ों से जोड़ती है, कमियों-अच्छाइयों का आईना दिखाती है, और प्रकृति-संस्कृति को सहेजती है। हिंदी और पंजाबी में लिखना घर की खिड़की खोलकर ताज़ी हवा लेने जैसा है। प्रेमचंद, यशपाल, बच्चन, प्रसाद, निराला, रेणु, महादेवी, गुप्त, नागर, भारती, गुलज़ार, अमृता प्रीतम, शिव कुमार बटालवी, नानक सिंह—इन लेखकों ने साबित किया कि लेखन ज़िंदगी को जीवंत करता है।
तो अगली बार जब आप कलम उठाएँ, याद रखें—आप अपनी मिट्टी की खुशबू, संस्कृति का रंग, और ज़िंदगी का आलम लिख रहे हैं। यह जादू हर पाठक को छूता है, जड़ों से जोड़ता है, और इंसानियत को ज़िंदा रखता है। लिखते रहिए, क्योंकि लेखन ही वह कला है, जो हमें इंसान बनाए रखती है।
