लिखने की कला: शब्दों में बुनते सपने और सच्चाई
CHAIFRY POT
लिखने की कला: भाग -2
7/12/20251 min read
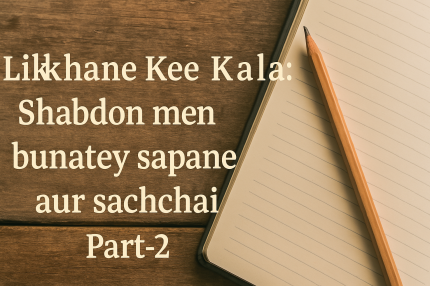
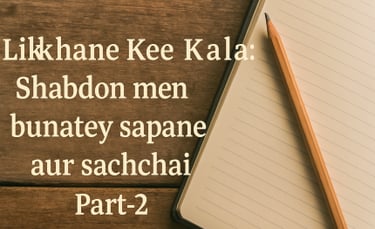
शब्दों में रचना करना एक ऐसी कला है, जो मन के सपनों को हकीकत के रंगों से सजाती है। चाहे वह हिंदी की खड़ीबोली हो, पंजाबी की मधुर लय, बंगाली की गीतमयी गहराई, मराठी की माटी की सुगंध, मलयालम की शांत लहरें, या आदिवासी समाज की मौखिक कथाएँ, लेखन हमें अपनी कल्पनाओं को आज़ादी देने और अपनी सच्चाई को बयान करने का रास्ता देता है।यह एक ऐसा दर्पण है, जिसमें हम अपने मन की उड़ान, अपनी ज़िंदगी की सच्चाई, और अपनी जड़ों की गहराई को देख सकते हैं। यह लेख उस रचनात्मकता की बात करता है—कैसे शब्द हमारे सपनों को पंख देते हैं, हमारी हकीकत को उजागर करते हैं, और हमें अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाने की ताकत देते हैं।
रचना करना ऐसा है जैसे चाँदनी रात में किसी नदी किनारे बैठकर तारों के साथ कहानी गढ़ना। हर शब्द एक किरण है, जो अपने साथ एक सपना, एक भावना, या एक सत्य लिए चमकता है। जब कोई लेखक अपनी कलम उठाता है, तो वह सिर्फ़ अक्षर नहीं उकेरता; वह अपने मन की गहराइयों, अपने गाँव की गलियों, शहर की चहल-पहल, या जंगल की सघन शांति को कागज़ पर उतारता है। चाहे वह प्रेम की कविता हो, जिसमें दिल की धड़कनें गूँजती हों, या एक कहानी, जिसमें गाँव की सादगी बसी हो, हर रचना लेखक के मन का एक टुकड़ा होती है। हिंदी में रचना करना तो जैसे किसी पुराने दोस्त के साथ चाय की प्याली थामे बातें करना है—सहज, अपनेपन से भरा। खड़ीबोली, हमारी रोज़मर्रा की ज़ुबान, गाँव की चौपाल से लेकर शहर की कॉफी शॉप तक हर जगह बसती है। इसमें नानी की लोरियों की मिठास है, तो मेट्रो में बैठे नौजवान की गपशप भी। इसकी सरलता हर पाठक के दिल को छू लेती है।
क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपने सपनों को हकीकत में बदलने की सोची है? वह पल, जब कल्पनाएँ आसमान को छूने लगती हैं, और मन में अनगिनत कहानियाँ जन्म लेती हैं। रचना करना उन पलों को कागज़ पर उतारने का हुनर है। प्रेमचंद की ‘गोदान’ में होरी का अपने खेत और बैलों का सपना, उसकी मेहनत और हार, सब कुछ इतनी सच्चाई से उकेरा गया है कि आप उस गाँव की मिट्टी को छू सकते हैं। यशपाल की ‘झूठा सच’ में आज़ादी के सपने और उस दौर की कड़वी हकीकत का चित्रण आपको इतिहास की गलियों में ले जाता है। ये लेखक सिर्फ़ कहानियाँ नहीं रचते; वे सपनों को सच्चाई से जोड़ते हैं।
पंजाबी साहित्य में यह सपनों और सच्चाई का मेल खूब झलकता है। अमृता प्रीतम की ‘अज्ज आखां वारिस शाह नूं’ बँटवारे की पीड़ा को बयान करती है, मगर एक बेहतर कल का सपना भी दिखाती है। उनकी कविताएँ पंजाब के खेतों की हरियाली और वहाँ के लोगों के दर्द को इतनी गहराई से उकेरती हैं कि आप उस माहौल में डूब जाते हैं। शिव कुमार बटालवी की ‘माये नि माये’ प्रेम और विरह के सपनों को पंजाब की नदियों और खेतों के साथ गीतों की तरह बुनती है। नानक सिंह की ‘चित्रलेखा’ में पंजाब के गाँवों की ज़िंदगी, मेहनत, और सुख-दुख इतने सुंदर ढंग से उभरते हैं कि आप उन गलियों में चल पड़ते हैं।
बंगाली साहित्य में रवींद्रनाथ टैगोर की कविताएँ, जैसे ‘गीतांजलि’, सपनों और सत्य का एक अनूठा मेल पेश करती हैं। उनकी पंक्तियाँ, “जहाँ मन भय से मुक्त हो”, एक ऐसी दुनिया का सपना दिखाती हैं, जहाँ सच्चाई और स्वतंत्रता सर्वोपरि हैं। बंगाल की नदियों और खेतों की हरियाली उनकी रचनाओं में जीवंत हो उठती है। मराठी साहित्य में पु. ल. देशपांडे की कहानियाँ, जैसे ‘बटाट्याची चाल’, आम ज़िंदगी के सपनों और हास्य भरी सच्चाई को बयान करती हैं। उनकी लेखनी में मराठी माटी की सादगी और हँसी-मज़ाक की चटपटाहट झलकती है। मलयालम में वैकोम मुहम्मद बशीर की ‘बाल्यकाला सखी’ में ग्रामीण जीवन की सादगी, प्रेम के सपने, और सामाजिक सच्चाई का ऐसा चित्रण है कि आप केरल के गाँवों की हवा में साँस लेने लगते हैं।
आदिवासी समाज की मौखिक परंपराएँ भी सपनों और सच्चाई का अनूठा खजाना हैं। संथाल समुदाय की लोककथाएँ, जैसे “बोंगा” (आदिवासी देवता) की कहानियाँ, प्रकृति और मानव के रिश्ते को सपनों की तरह बयान करती हैं। इन कथाओं में जंगल, नदियाँ, और आदिवासी जीवन की सादगी और संघर्ष साफ झलकते हैं। गोंड समुदाय की कहानियाँ, जैसे “बारा मसीहा” (बारह मसीहाओं की कथा), प्रकृति के साथ उनके गहरे रिश्ते और जीवन की सच्चाई को दर्शाती हैं। ये मौखिक रचनाएँ, जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, आदिवासी समाज के सपनों—प्रकृति के साथ सामंजस्य, समुदाय की एकता—और उनकी सच्चाई—संघर्ष और जीवटता—को जीवंत करती हैं।
रचना करना सिर्फ़ सपने बुनना नहीं, बल्कि सच्चाई को सामने लाना भी है। सूरदास की भक्ति कविताएँ, जो कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति की सच्चाई को बयान करती हैं, पाठक को आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाती हैं। कबीर के दोहे समाज की रूढ़ियों पर चोट करते हैं। उनकी पंक्तियाँ, “मोको कहाँ ढूँढे रे बन्दे, मैं तो तेरे पास में”, सादगी और सत्य की खोज की ओर ले जाती हैं। तुलसीदास की ‘रामचरितमानस’ में राम के आदर्श और नैतिकता की सच्चाई हर चौपाई में झलकती है। “सियाराम मय सब जग जानी” जैसी पंक्तियाँ हमें जीवन के मूल्यों से जोड़ती हैं।
आधुनिक हिंदी लेखकों में हरिवंश राय बच्चन की ‘मधुशाला’ जीवन के फलसफे को सपनों के रंग में पेश करती है। “मधुशाला की मधुर माया, सबको बाँधे एक सूत्र में” जैसी पंक्तियाँ एकता और प्रेम के सपने को ज़िंदा रखती हैं। मैथिलीशरण गुप्त की ‘भारत-भारती’ देशप्रेम के सपनों को सच्चाई से जोड़ती है, जहाँ देश की मिट्टी का गर्व हर शब्द में बस्ता है। गुलज़ार की कविताएँ, जैसे “दिल ढूँढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन”, आधुनिक ज़िंदगी में पुरानी सादगी के सपने को जीवंत करती हैं। उनकी ‘रात पश्मीने की’ में पंजाब की ठंड और गाँवों की सादगी का अहसास है।
बंगाली में शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की ‘देवदास’ प्रेम के सपनों और सामाजिक बंधनों की सच्चाई को उजागर करती है। मराठी में वि. स. खांडेकर की ‘ययाति’ मानव की इच्छाओं और नैतिकता के बीच के द्वंद्व को दर्शाती है। मलयालम में ओ. चंदूमेनन की ‘इंदुलेखा’ प्रेम और सामाजिक परिवर्तन के सपनों को केरल की सांस्कृतिक सच्चाई के साथ जोड़ती है। आदिवासी समाज में मुंडा समुदाय की लोककथा “सिंगबोंगा” प्रकृति के साथ उनके गहरे रिश्ते और सामुदायिक जीवन की सच्चाई को बयान करती है। ये सभी रचनाएँ सपनों और सच्चाई को अलग-अलग रंगों में पेश करती हैं।
प्रकृति रचना में सपनों और सच्चाई का मेल बनाती है। सुमित्रानंदन पंत की कविताएँ हिमालय की शांति और हरियाली को सपनों की तरह उकेरती हैं। “हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर” जैसी पंक्तियाँ प्रकृति की खूबसूरती को जीवंत करती हैं। जयशंकर प्रसाद की ‘कामायनी’ में प्रकृति और मानव की भावनाएँ एक साथ रंग बिखेरती हैं। महादेवी वर्मा की “मैं नीर भरी दुख की बदली” बारिश और बादलों के ज़रिए मानव के दुख और सपनों को बयान करती है। पंजाबी में शिव कुमार बटालवी की ‘लूणा’ पंजाब के खेतों और प्रेम की कहानी को सपनों के रंग में रंगती है। बंगाली में जिबानानंद दास की कविताएँ, जैसे “बनलता सेन”, बंगाल की ग्रामीण सादगी और सपनों को प्रकृति के साथ जोड़ती हैं। मराठी में कुसुमाग्रज की कविताएँ प्रकृति और मानव जीवन की सच्चाई को दर्शाती हैं। मलयालम में ताकज़ी शिवशंकर पिल्लई की ‘चेम्मीन’ समुद्र और मछुआरों की ज़िंदगी के सपनों और सच्चाई को बयान करती है। आदिवासी गोंड कथाओं में जंगल और नदियाँ सपनों के प्रतीक हैं, जो उनके जीवन की सादगी और संघर्ष को दर्शाती हैं।
रचना हमें अपनी ज़िंदगी की सच्चाई को समझने का मौका देती है। सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ की ‘राम की शक्ति पूजा’ में मानव की आंतरिक ताकत और संघर्ष की सच्चाई झलकती है। फणीश्वरनाथ रेणु की ‘मारे गए गुलफाम’ में गाँव की मासूमियत और कमियाँ इतनी खूबसूरती से उकेरी गई हैं कि आप उस गाँव की गलियों में खो जाते हैं। भैरव प्रसाद गुप्त की ‘सतह से उठता हुआ आदमी’ मेहनतकशों की उम्मीद और जद्दोजहद की सच्चाई को दिखाती है। अमृतलाल नागर की ‘बूँद और समुद्र’ में आम ज़िंदगी की छोटी-छोटी बातें इतनी सादगी से बयान होती हैं कि पाठक उन किरदारों के साथ हँसता-रोता है। पंजाबी में नानक सिंह की ‘पवित्र पापी’ गाँव की ज़िंदगी की अच्छाइयों और कमियों को सादगी से दर्शाती है। अमृता प्रीतम की ‘पिंजर’ औरतों की ताकत और पीड़ा की सच्चाई को सामने लाती है। बंगाली में बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय की ‘आनंदमठ’ देशप्रेम के सपनों और औपनिवेशिक दौर की सच्चाई को उजागर करती है। मराठी में ना. सी. फडके की कहानियाँ आम ज़िंदगी की सादगी और सच्चाई को बयान करती हैं। मलयालम में एम. टी. वासुदेवन नायर की ‘नालुकेट्टु’ पारिवारिक जीवन की सच्चाई और सपनों को दर्शाती है। आदिवासी संथाल कथाएँ, जैसे “मारंग बुरु” की कहानी, प्रकृति और समुदाय की सच्चाई को सामने लाती हैं।
हिंदी की खड़ीबोली में रचना करना किसी अपने से दिल की बात कहने जैसा है। यह भाषा गाँव की चौपाल से लेकर शहर की कॉफी शॉप तक हर जगह बोली जाती है। धर्मवीर भारती की ‘गुनाहों का देवता’ प्रेम और ज़िंदगी की उलझनों को इतनी सहजता से बयान करती है कि पाठक उसमें डूब जाता है। पंजाबी में अमृता प्रीतम, शिव कुमार बटालवी, और नानक सिंह की रचनाएँ गाँव की ज़िंदगी को दिल तक पहुँचाती हैं। बंगाली, मराठी, मलयालम, और आदिवासी मौखिक कथाएँ भी अपनी-अपनी ज़ुबान में सपनों और सच्चाई को बयान करती हैं।
आज के डिजिटल दौर में रचना का रूप बदल गया है। लोग ब्लॉग, सोशल मीडिया, और वीडियो के ज़रिए अपनी बात कह रहे हैं। गुलज़ार की तरह, जो अपनी कविताओं में पुरानी यादों और नए सपनों को पिरोते हैं, आज के लेखक भी अपनी सच्चाई को नए अंदाज़ में पेश करते हैं। उनकी ‘रात पश्मीने की’ में पंजाब की सादगी और ठंड का अहसास है। आदिवासी समुदायों में मौखिक कथाएँ अब लिखित रूप ले रही हैं, जैसे संथाल लेखक हंसदा सोवेंद्र शेखर की ‘द आदिवासी विल नॉट डांस’, जो आदिवासी जीवन की सच्चाई और सपनों को बयान करती है।
रचनात्मकता का भविष्य सुनहरा है। जब तक इंसान हैं, सपने होंगे, और जब तक सपने होंगे, रचना ज़िंदा रहेगी। यह कला हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है, हमारी सच्चाई को सामने लाती है, और हमें अपने सपनों को उड़ान देने का हौसला देती है। हिंदी, पंजाबी, बंगाली, मराठी, मलयालम, और आदिवासी कथाओं के लेखकों—प्रेमचंद, यशपाल, बच्चन, प्रसाद, निराला, रेणु, महादेवी, गुप्त, नागर, भारती, गुलज़ार, टैगोर, देशपांडे, बशीर, अमृता प्रीतम, शिव कुमार बटालवी, नानक सिंह—ने दिखाया है कि रचना सपनों और सच्चाई का मेल है।
तो अगली बार जब आप कलम उठाएँ, याद रखें—आप सिर्फ़ शब्द नहीं लिख रहे, आप अपने सपनों को उड़ान दे रहे हैं, अपनी सच्चाई को बयान कर रहे हैं। यह रचनात्मकता हर पाठक को छूती है, और यही है लेखन की कला का असली कमाल। रचते रहिए, क्योंकि यह कला हमें इंसान बनाए रखती है।
