लखनऊ की तहजीब : “पहले आप” से “का हाल बा” तक
CHAIFRY POT
Chaifry
7/6/20251 min read
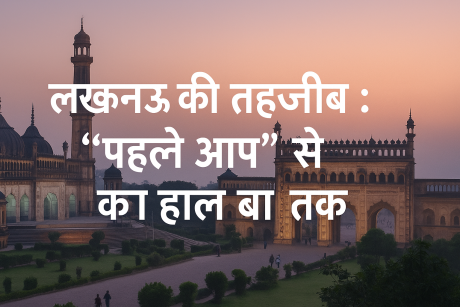
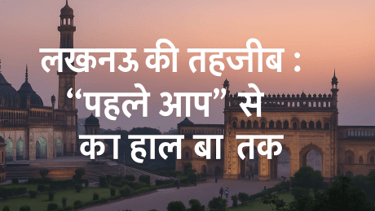
लखनऊ, वह नगरी, जहाँ नवाबों की शान और गंगा-जमुनी तहजीब का आलम एक मधुर राग की तरह गूँजता है, साहित्य और भाषा का वह दीपस्तंभ है, जिसकी रोशनी ने सदियों तक हिंदुस्तान के सांस्कृतिक आकाश को आलोकित किया। यह शहर, जहाँ अवधी की मधुर लय, उर्दू की नफ़ीस रवानी, और हिंदी की सौम्यता एक साथ साँस लेती हैं, अपनी शालीनता, नजाकत, और समन्वय के लिए विश्वविख्यात है। लखनऊ की गलियों में “पहले आप” की शिष्टता बसती है, और हवाओं में मीर की ग़ज़लों, अनीस की मरसियों, दाग़ की नज़्मों, मजाज़ की इंक़लाबी शायरी, और हिंदी साहित्य की रचनाओं की खुशबू तैरती है। मगर आज, इस तहजीब का सुनहरा आलम कुछ मद्धम पड़ता नज़र आता है। इसकी भाषा और साहित्य, जो कभी इस नगरी की रूह थे, अब समय की आँधी में अपनी चमक खोते दिख रहे हैं।
यह लेख लखनऊ की तहजीब, भाषा, और साहित्य को साहित्यिक दृष्टि से देखता है, इसकी गिरावट के कारणों का गहन विश्लेषण करता है, लखनऊ के हिंदी साहित्य में योगदान को रेखांकित करता है, और उन शायरों और साहित्यकारों की अमर रचनाओं को याद करता है, जिन्होंने इस शहर को साहित्य का तिलस्मी ताज़ पहनाया।
लखनऊ की तहजीब: एक काव्यात्मक चित्र
लखनऊ की तहजीब कोई साधारण सांस्कृतिक धरोहर नहीं, बल्कि एक जीवंत काव्य है, जो शब्दों की सैर, लहजों की लय, और व्यवहार की नफासत में ढला है। यहाँ की गलियाँ—अमीनाबाद की रौनक, हज़रतगंज की चहल-पहल, चौक की पुरानी हवेलियाँ, और कैसरबाग़ की नवाबी शान—कभी साहित्यिक मंच थीं, जहाँ रात की चाँदनी में मुशायरे खिलते थे, और शब्दों की माला में भावनाएँ पिरोई जाती थीं। नवाबी दौर में लखनऊ ने उर्दू और हिंदी साहित्य को वह शिखर प्रदान किया, जो किसी अन्य शहर को नसीब नहीं हुआ। अवधी, जो इस अंचल की जन-जन की ज़बान थी, अपनी मधुर लय और काव्यात्मक प्रवाह के साथ साहित्य की नींव बनी। मलिक मुहम्मद जायसी की पद्मावत ने अवधी को प्रेम और आध्यात्म का काव्य बनाया, तो तुलसीदास की रामचरितमानस ने इसे भक्ति की गंगा में डुबो दिया।
उर्दू, जो नवाबी शासन के दौरान इस नगरी में पनपी, ने लखनऊ की भाषा को एक नफ़ीस रंग दिया। यहाँ का लहजा, जिसमें “जनाब”, “हुज़ूर”, और “आप” जैसे शब्दों की शालीनता थी, मानो एक शेर का मिसरा हो। बातचीत में एक काव्यात्मक लय थी, जैसे हर वाक्य में शायरी का जादू छिपा हो। नवाब वाजिद अली शाह, जो स्वयं एक कवि और कथक के संरक्षक थे, ने लखनऊ को साहित्य और कला का मरकज़ बनाया। उनकी रचनाएँ, जैसे “बाहर-ए-इश्क़ में हर चीज़ बे-क़रार है,” प्रेम और नजाकत की मिसाल थीं। लखनऊ की तहजीब में हिंदू-मुस्लिम एकता का वह सुंदर समन्वय था, जो दशहरा और दीवाली के साथ ईद और मुहर्रम के उत्सव में झलकता था। यह समन्वय साहित्य में भी दिखता था, जहाँ अवधी, उर्दू, और हिंदी ने मिलकर एक ऐसी ज़बान रची, जो दिलों को जोड़ती थी।
लखनऊ का साहित्यिक वैभव: उर्दू शायरी का आलम
लखनऊ का साहित्यिक परिदृश्य उर्दू शायरी का वह तारों भरा आकाश है, जिसमें मीर तकी मीर, मिर्ज़ा अनीस, दाग़ देहलवी, और मजाज़ लखनवी जैसे सितारे जगमगाए। मीर, जिन्हें “ख़ुदा-ए-सुख़न” की उपाधि मिली, ने अपनी ग़ज़लों में प्रेम की तड़प, ज़िंदगी की नश्वरता, और इंसानी जज़्बात की गहराई को इस तरह उकेरा कि उनकी पंक्तियाँ आज भी दिलों को बेचैन करती हैं। उनकी ग़ज़ल, “दिल-ए-नादाँ तुझे हुआ क्या है, आख़िर इस दर्द की दवा क्या है,” लखनऊ की तहजीब की नफासत और भावनात्मक गहराई का प्रतीक है। मीर की शायरी में लखनऊ की वह रूह बसती है, जो शालीनता और दर्द का मिश्रण थी।
मिर्ज़ा अनीस ने मरसिया को एक नई साहित्यिक ऊँचाई दी। उनकी मरसियाँ, जो करबला की त्रासदी को बयान करती थीं, केवल शोकगीत नहीं थीं, बल्कि काव्य की वह कृति थीं, जिनमें शब्दों का चयन, लय, और भावनाओं का प्रवाह लखनऊ की साहित्यिक परंपरा को परिभाषित करता था। अनीस की पंक्तियाँ, जैसे “जब क़ता की मसीह ने एक नज़र देखा, हर ज़ख़्म से रौशनी की किरण निकली,” काव्य और आध्यात्म का अनूठा संगम थीं।
दाग़ देहलवी ने लखनऊ की ग़ज़ल को सादगी और नजाकत का नया रंग दिया। उनकी शायरी में लखनवी तहजीब की वह शालीनता थी, जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उनकी पंक्ति, “ज़िंदगी यूं भी गुज़र ही जाती, क्यों तेरा रहगुज़र याद आया,” प्रेम और विरह की उस नाज़ुक भावना को बयान करती है, जो लखनऊ की तहजीब का हिस्सा थी।
मजाज़ लखनवी, जिन्हें “शायर-ए-इंक़लाब” कहा जाता है, ने लखनऊ की साहित्यिक परंपरा में एक नया रंग जोड़ा। उनकी नज़्म “आवारा” लखनऊ की रातों, गलियों, और तहजीब का एक जीवंत चित्र खींचती है:
सहरा में आवारा, बस्ती में आवारा
हर सिम्त ठोकर खाता फिरता हूँ बेकार
मजाज़ की शायरी में लखनऊ की वह रूह झलकती है, जो शालीनता और बग़ावत का मिश्रण थी। उनकी नज़्में, जैसे “नौजवान ख़ातून से,” युवा जोश और सामाजिक बदलाव की पुकार थीं, जो लखनऊ की नई पीढ़ी को प्रेरित करती थीं। मजाज़ ने लखनऊ की तहजीब को एक आधुनिक स्वर दिया, जिसमें प्रेम, विद्रोह, और सौंदर्य का समन्वय था।
लखनऊ का हिंदी साहित्य में योगदान
लखनऊ की साहित्यिक धरोहर केवल उर्दू शायरी तक सीमित नहीं है; इस नगरी ने हिंदी साहित्य को भी अपार समृद्धि प्रदान की है। लखनऊ हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जहाँ आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास में कई महान साहित्यकारों ने योगदान दिया। हिंदी साहित्य में लखनऊ का योगदान अवधी और ब्रज भाषा के माध्यम से शुरू हुआ, जो बाद में खड़ी बोली हिंदी के विकास में परिलक्षित हुआ।
तुलसीदास, जिनकी रामचरितमानस हिंदी साहित्य की अमर कृति है, ने अवधी को एक साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित किया। उनकी रचनाएँ लखनऊ की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का हिस्सा हैं। रामचरितमानस ने न केवल भक्ति साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि अवधी भाषा को एक साहित्यिक गरिमा प्रदान की। तुलसीदास की पंक्तियाँ, जैसे “रामचरितमानस सरवर, सुमति सुभाग्य सुठाम,” आज भी लखनऊ की साहित्यिक परंपरा की नींव हैं।
आधुनिक हिंदी साहित्य में लखनऊ का योगदान भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग से और स्पष्ट हुआ। हालाँकि भारतेंदु बनारस से थे, लखनऊ हिंदी साहित्य के विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा। लखनऊ में हिंदी साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं और साहित्यिक सभाओं ने आधुनिक हिंदी को बढ़ावा दिया। 20वीं सदी में, लखनऊ के साहित्यकारों ने छायावाद, प्रगतिवाद, और नई कविता जैसे आंदोलनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
सुमित्रानंदन पंत, जो छायावाद के प्रमुख कवि थे, ने लखनऊ में कुछ समय बिताया और यहाँ की सांस्कृतिक समृद्धि से प्रभावित हुए। उनकी कविता “ग्राम श्री” प्रकृति और मानव भावनाओं का सुंदर चित्रण करती है, और इसमें लखनऊ की तहजीब की छाया देखी जा सकती है। महादेवी वर्मा, छायावाद की एक अन्य स्तंभ, ने भी लखनऊ को अपनी साहित्यिक यात्रा का हिस्सा बनाया। उनकी कविताएँ, जैसे “मैं नीर भरी दुख की बदली,” प्रेम और वेदना की गहराई को व्यक्त करती हैं, जो लखनऊ की नफ़ीस तहजीब के साथ मेल खाती हैं।
लखनऊ ने प्रगतिवादी साहित्य को भी समृद्ध किया। यशपाल और अमृतलाल नागर जैसे लेखकों ने लखनऊ को अपनी रचनाओं का केंद्र बनाया। यशपाल का उपन्यास दादा कामरेड सामाजिक बदलाव और क्रांतिकारी विचारों का प्रतीक है, जो लखनऊ की इंक़लाबी भावना से प्रेरित था। अमृतलाल नागर की रचनाएँ, जैसे बूँद और समुद्र, लखनऊ की लोक संस्कृति और तहजीब को चित्रित करती हैं। उनकी कहानियाँ और उपन्यास लखनऊ की गलियों, बाज़ारों, और सामाजिक जीवन को जीवंत करते हैं।
लखनऊ की हिंदी पत्रकारिता ने भी हिंदी साहित्य को बढ़ावा दिया। कवि वचन सुधा और हिंदुस्तानी जैसी पत्रिकाएँ लखनऊ से प्रकाशित होती थीं और हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। लखनऊ विश्वविद्यालय और अन्य साहित्यिक संस्थानों ने हिंदी साहित्य को एक मज़बूत आधार प्रदान किया।
तहजीब और साहित्य में मद्धम पड़ती चमक
लखनऊ की तहजीब और साहित्य की वह चमक, जो कभी इस नगरी का गहना थी, आज कुछ मद्धम पड़ती दिख रही है। इसकी भाषा, जो शायरी और काव्य की बुनियाद थी, अब रोज़मर्रा की बोलचाल में एक नया रंग ले रही है। लखनऊ की गलियों में “हुज़ूर” और “जनाब” की जगह अब भोजपुरी की बेबाकी लिए “का हाल बा?” और “काहे” जैसे शब्द गूँजते हैं। यह बदलाव पूर्वांचल के प्रभाव का परिणाम है, जहाँ भोजपुरी की जीवंतता और स्पष्टवादिता ने लखनऊ की नफ़ीस अवधी-उर्दू को चुनौती दी है। भोजपुरी, जो अपनी लोकप्रियता और सादगी के लिए मशहूर है, लखनऊ की शालीन ज़बान से टकराती है। यह टकराव साहित्य में भी दिखता है, जहाँ भोजपुरी गीतों और सिनेमा की रौनक ने उर्दू ग़ज़ल, अवधी काव्य, और हिंदी साहित्य को पृष्ठभूमि में धकेल दिया है।
यह मद्धम पड़ती चमक केवल भाषाई नहीं, बल्कि साहित्यिक और सांस्कृतिक भी है। लखनऊ के मुशायरे, जो कभी रात की चाँदनी में शब्दों के फूल बिखेरते थे, अब गिनती के आयोजनों तक सिमट गए हैं। कथक की थिरकन और शास्त्रीय संगीत की स्वरलहरियाँ अब भोजपुरी गीतों और आधुनिक पॉप की चकाचौंध में दब रही हैं। मीर की ग़ज़लें, अनीस की मरसियाँ, दाग़ की नज़्में, मजाज़ की इंक़लाबी शायरी, और तुलसीदास की भक्ति कविता अब किताबों की धूल भरी अलमारियों और पुरानी यादों में कैद हो रही हैं। नई पीढ़ी का इनसे रिश्ता कमज़ोर पड़ गया है, क्योंकि आधुनिकता की चमक ने उनकी आँखों को चौंधिया दिया है।
आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण ने इस गिरावट को और गहरा किया है। अंग्रेजी और हिंदी का बढ़ता प्रभाव, सोशल मीडिया की तेज़ रफ़्तार, और पश्चिमी संस्कृति का आकर्षण ने लखनऊ की भाषा और साहित्य को हाशिए पर ला दिया है। लखनऊ की तहजीब का आधार उसकी समावेशिता थी, जो गंगा-जमुनी तहजीब के रूप में फलती-फूलती थी। मगर आज, सामाजिक और क्षेत्रीय ध्रुवीकरण ने इस समन्वय को कमज़ोर किया है। पूर्वांचल की मानसिकता, जिसमें क्षेत्रीय गर्व और बेबाकी का रंग है, लखनऊ की नफ़ीस शालीनता से टकराती है। भोजपुरी सिनेमा और गीत, जो अपनी सादगी और हास्य के लिए जाने जाते हैं, कई बार अपनी अश्लीलता के लिए आलोचना का शिकार होते हैं, जो लखनऊ की साहित्यिक नजाकत से मेल नहीं खाता।
हिंदी साहित्य भी इस गिरावट से अछूता नहीं रहा। लखनऊ में हिंदी साहित्यिक सभाएँ और पत्रिकाएँ, जो कभी साहित्यकारों का मेला थीं, अब कम हो गई हैं। तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, और महादेवी वर्मा की रचनाएँ अब स्कूलों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों तक सिमट गई हैं। नई पीढ़ी का ध्यान सोशल मीडिया और डिजिटल मनोरंजन की ओर अधिक है, जिसके कारण हिंदी साहित्य की समृद्ध परंपरा धूमिल पड़ रही है।
क्या यह चमक फिर से लौट सकती है?
लखनऊ की तहजीब और साहित्य में मद्धम पड़ती यह चमक क्या अपरिवर्तनीय है? यह सवाल मन को बेचैन करता है। मगर लखनऊ का इतिहास हमें आशा की किरण दिखाता है। यह नगरी कई तूफानों से गुज़री है—नवाबी युग का पतन, ब्रिटिश शासन की सख्ती, स्वतंत्रता संग्राम की उथल-पुथल, और आधुनिकता की तेज़ रफ़्तार—फिर भी इसने अपनी साहित्यिक रूह को संजोया है। मीर की ग़ज़लें, अनीस की मरसियाँ, दाग़ की नज़्में, मजाज़ की इंक़लाबी शायरी, और तुलसीदास की भक्ति कविता आज भी इस नगरी की साहित्यिक धरोहर का गहना हैं।
भोजपुरी और अवधी, दोनों ही अवध की मिट्टी से उपजी ज़बानें हैं। इनमें टकराव नहीं, बल्कि समन्वय की संभावना है। भोजपुरी की जीवंतता, अवधी की मधुरता, और हिंदी की सौम्यता अगर एक साथ मिलें, तो लखनऊ का साहित्य एक नδया रंग ले सकता है। लखनऊ की तहजीब की ताकत उसकी लचीलापन में है। यह शहर हमेशा से नए प्रभावों को गले लगाता रहा है, और उन्हें अपनी नफासत के रंग में ढालता रहा है। मजाज़ की नज़्म “आवारा” में लखनऊ की रातों का ज़िक्र आज भी इस शहर की रूह को ज़िंदा करता है। अनीस की मरसियाँ, मीर की ग़ज़लें, और तुलसीदास की रामचरितमानस हमें याद दिलाती हैं कि लखनऊ की तहजीब केवल भाषा और साहित्य नहीं, बल्कि एक जीवनशैली है, जो शालीनता, नजाकत, और समन्वय का प्रतीक है।
